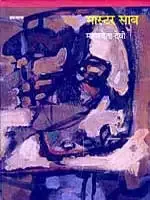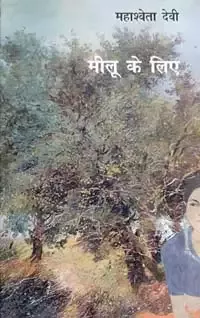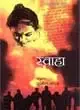|
सामाजिक >> मास्टर साब मास्टर साबमहाश्वेता देवी
|
544 पाठक हैं |
||||||
शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ निरंतर संघर्ष करने वाले गरीब एवं समर्पित स्कूल-मास्टर की आत्मीय कथा...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बांग्ला की यशस्वी साहित्यकार महाश्वेता
देवी के लिए शब्द और कर्म अलग-अलग नहीं हैं। उनका कर्म और उनकी सारी
चिंताएँ जहाँ शोषित एवं वंचित लोगों के लिए हैं, वहीं उनके समग्र सृजन के
केंद्र में भी शोषण के विरुद्ध तीव्र और सार्थक विद्रोह है। कहना न होगा
कि उसका साक्षी उनका यह उपन्यास ‘मास्टर साब’ भी है।
‘मास्टर साब’ एक जीवनी परक विचारोत्तेजक और मार्मिक
उपन्यास
है।
इस उपन्यास में शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ निरंतर संघर्ष करने वाले गरीब एवं समर्पित स्कूल मास्टर की आत्मीय व्यथा-कथा तो है ही, उनके बहाने महाश्वेता देवी ने साठ-सत्तर के दशक में उपजे नक्सलवादी आंदोलन की गतिविधियों और उसके वैचारिक सरोकारों को भी पूरे साहस के साथ प्रस्तुत किया है। दरअसल मास्टर साब की कहानी को कहने की कोशिश में महाश्वेता देवी ने समकालीन समाज और परिवेश की विसंगतियों के बीच एक साधारण चरित्र के जुझारू संकल्प को अपनी असाधारण लेखनी से प्रखर अभिव्यक्ति दी है। शिल्प और भाषा के स्तर पर इस अद्वितीय प्रयोगात्मक उपन्यास की प्रस्तुति निस्संदेह हिन्दी पाठकों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।
इस उपन्यास में शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ निरंतर संघर्ष करने वाले गरीब एवं समर्पित स्कूल मास्टर की आत्मीय व्यथा-कथा तो है ही, उनके बहाने महाश्वेता देवी ने साठ-सत्तर के दशक में उपजे नक्सलवादी आंदोलन की गतिविधियों और उसके वैचारिक सरोकारों को भी पूरे साहस के साथ प्रस्तुत किया है। दरअसल मास्टर साब की कहानी को कहने की कोशिश में महाश्वेता देवी ने समकालीन समाज और परिवेश की विसंगतियों के बीच एक साधारण चरित्र के जुझारू संकल्प को अपनी असाधारण लेखनी से प्रखर अभिव्यक्ति दी है। शिल्प और भाषा के स्तर पर इस अद्वितीय प्रयोगात्मक उपन्यास की प्रस्तुति निस्संदेह हिन्दी पाठकों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।
प्रस्तुति
भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से श्रीमती महाश्वेता देवी से अनुरोध किया गया कि
वे अपनी रचना हमें प्रदान करें ताकि पुरस्कार समर्पण समारोह के अवसर पर
उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया जा सके। हमारा मत है कि हिंदी में पुस्तक
उपलब्ध होने पर भारतीय भाषाओं में उसके अनुवाद की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।
इस प्रकार महाश्वेता देवी के कृतित्व की पहचान को देशव्यापी बनाने की दिशा
में, अन्य सहयोगी प्रकाशनों के साथ यह हमारा विनम्र प्रयास होगा।
इस पुस्तक को पढ़ना अपने-आप में एक गहरा अनुभव है। कितनी सरलता और सहजता से सामाजिक जीवन की विद्रूपताओं और विसंगतियों को रेखांकित किया जा सकता है, यह ‘मास्टर साब’ कृति से प्रमाणित होता है। महाश्वेता देवी की पैनी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता। मानव समाज की अनकही पीड़ा की पहचान और अन्याय व शोषण के विरुद्ध अनवरत संघर्ष में भी छलक पड़नेवाला चुटीला हास्य-व्यंग्य—उनकी रचना में वह सब कुछ है जो पाठक को अभिभूत करता है, उसके विवेक को झकझोरता है और बेहतर समाज की ओकर इंगित करता है।
महाश्वेता देवी की चिंता उन लोगों के लिए है जो एक असहिष्णु और उत्पीड़क समाज के शिकार हैं और प्रशंसक भाव उन सबके लिए है जो विरोध के स्वर को मुखर करते हैं। यह सोच उनके लेखन में निरंतर प्रवाहित होता है। इस लेखन की विशिष्टता का कारण है समाज के उपेक्षित और वंचित वर्गों के इतिहास में उनकी गहरी दिलचस्पी। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इन उपेक्षित वर्गों के साथ महाश्वेता देवी का तादात्म्य केवल लेखन तक ही सीमित नहीं है; पिछले कई दशकों से वे निर्धनों, विशेषकर आदिवासियों की स्थिति को सुधारने के सभी प्रयासों के सक्रिय समर्थन देती रही हैं।
भारतीय साहित्य-जगत् में उनकी छवि एक ऐसी लेखिका की है जिनके लेखन और जीवन के बीच कोई विभाजक सीमारेखा नहीं है। जो लिखा है, वही उन्होंने जिया भी है। महाश्वेता देवी की कृतियाँ अन्याय के विरुद्ध इंसान की लड़ाई के महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हैं। आदिवासी जीवन के संवेदात्मक चित्रण के लिए और शोषण के विरुद्ध आदिवासी जनजातियों के निरंतर संघर्ष के समर्थन में उनके अदम्य साहस के लिए हम उन्हें नमन करते हैं। विश्वास है, महाश्वेतादेवी की यह कृति भी पाठकों को बहुत भाएगी।
प्रामाणिक अनुवाद के लिए डॉ.रणजीत साहा को मैं धन्यवाद देता हूँ—बधाई भी। पुस्तक के प्रकाशन में भारतीय ज्ञानपीठ के मेरे सहयोगी, श्री पद्मधर त्रिपाठी और डॉ. गुलाबचंद्र जैन ने जो निष्ठा व तत्परता दिखाई है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।
आशा है, ‘मास्टर साब’ घर-घर पहुँचेंगे और सभी के आत्मीय हो जाएँगे।
इस पुस्तक को पढ़ना अपने-आप में एक गहरा अनुभव है। कितनी सरलता और सहजता से सामाजिक जीवन की विद्रूपताओं और विसंगतियों को रेखांकित किया जा सकता है, यह ‘मास्टर साब’ कृति से प्रमाणित होता है। महाश्वेता देवी की पैनी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता। मानव समाज की अनकही पीड़ा की पहचान और अन्याय व शोषण के विरुद्ध अनवरत संघर्ष में भी छलक पड़नेवाला चुटीला हास्य-व्यंग्य—उनकी रचना में वह सब कुछ है जो पाठक को अभिभूत करता है, उसके विवेक को झकझोरता है और बेहतर समाज की ओकर इंगित करता है।
महाश्वेता देवी की चिंता उन लोगों के लिए है जो एक असहिष्णु और उत्पीड़क समाज के शिकार हैं और प्रशंसक भाव उन सबके लिए है जो विरोध के स्वर को मुखर करते हैं। यह सोच उनके लेखन में निरंतर प्रवाहित होता है। इस लेखन की विशिष्टता का कारण है समाज के उपेक्षित और वंचित वर्गों के इतिहास में उनकी गहरी दिलचस्पी। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इन उपेक्षित वर्गों के साथ महाश्वेता देवी का तादात्म्य केवल लेखन तक ही सीमित नहीं है; पिछले कई दशकों से वे निर्धनों, विशेषकर आदिवासियों की स्थिति को सुधारने के सभी प्रयासों के सक्रिय समर्थन देती रही हैं।
भारतीय साहित्य-जगत् में उनकी छवि एक ऐसी लेखिका की है जिनके लेखन और जीवन के बीच कोई विभाजक सीमारेखा नहीं है। जो लिखा है, वही उन्होंने जिया भी है। महाश्वेता देवी की कृतियाँ अन्याय के विरुद्ध इंसान की लड़ाई के महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हैं। आदिवासी जीवन के संवेदात्मक चित्रण के लिए और शोषण के विरुद्ध आदिवासी जनजातियों के निरंतर संघर्ष के समर्थन में उनके अदम्य साहस के लिए हम उन्हें नमन करते हैं। विश्वास है, महाश्वेतादेवी की यह कृति भी पाठकों को बहुत भाएगी।
प्रामाणिक अनुवाद के लिए डॉ.रणजीत साहा को मैं धन्यवाद देता हूँ—बधाई भी। पुस्तक के प्रकाशन में भारतीय ज्ञानपीठ के मेरे सहयोगी, श्री पद्मधर त्रिपाठी और डॉ. गुलाबचंद्र जैन ने जो निष्ठा व तत्परता दिखाई है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।
आशा है, ‘मास्टर साब’ घर-घर पहुँचेंगे और सभी के आत्मीय हो जाएँगे।
नई दिल्ली
27 मार्च, 1997
27 मार्च, 1997
दिनेश मिश्र
मानद निदेशक
मानद निदेशक
निवेदन
1996 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा के साथ श्री दिनेश एक पांडुलिपि भेज
देने का अनुरोध किया था ताकि वे इसका हिंदी अनुवाद पुस्तकाकर प्रकाशित कर
सकें। 1979 में शारदीया ‘प्रमा’ में मेरा एक उपन्यास
प्रकाशित
हुआ था—‘मास्टर साब’। मैं इस कृति को
विस्तार से लिखना
चाहती थी लेकिन मुझे दोबारा समय नहीं मिल पाया। श्री दिनेश मिश्र ने जब
कृति भेजने का अनुरोध किया था तब ‘मास्टर
साब’ उपन्यास
भेजते हुए मुझे जो थोड़ा-बहुत संकोच हो रहा था, उसे अख्तर-उज़-ज़मान के
टेलिग्राम ने दूर कर दिया। उनका निधन अभी-अभी 4 जनवरी 1997 को 53 वर्ष की
आयु में हो गया। इस कृति को लेकर अक्सर मेरी उनसे बातें होती रही हैं।
उनसे होने वाली बातों से मुझे जान पड़ा कि हम दोनों के विश्वास का एक ही
आधार रहा है। हालाँकि मैं जिन्हें जानती-पहचानती हूँ वे लेखक के तौर पर
प्रतिष्ठित अख़्तर-उज़-ज़मान हैं मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल हो या
कि बांग्ला देश, वे इस क्षेत्र के श्रेष्ठ उपन्यास लेखक हैं। मुझसे कई
गुना बड़े लेखक और यह बात मैं कई बार ‘बांग्ला देश’
विषयक
अपने उन चार आलेखों में भी दोहरा चुकी हूँ— जो कभी
‘आजकल’ पत्र में प्रकाशित हुए थे।
‘मास्टर साब’, जैसा कि स्पष्ट ही है, एक जीवनीपरक उपन्यास है। मैंने इस से कभी इनकार नहीं किया कि’70 के दशक से जुड़े आंदोलन को मैंने अपना भरपूर समर्थन दिया था। बिहार का आरा जिला वर्ष 1857-58 के दौरान वीर कुअँर सिंह का जिला रहा है। ’70 के दशक में जगदीश मास्टर में धनी जोतदारों द्वारा हरिजन लड़कियों के ऊपर किए जा रहे शोषण और उत्पीड़न के विरुपद्ध अपना प्रतिवाद जताया था। उन्होंने ‘हरिजनिस्तान’ नामक एक गीत-संकलन प्रकाशित किया था और उनके सहोगियों में शहर में एक मशाल जुलूस भी निकाला था। उनका नारा था—‘हरिजनिस्तान लेकर रहेंगे’। यह और कुछ नहीं, रूढ़िवादी अंध-व्यवस्था के विरुद्ध संगठित विद्रोह था और मास्टर साब इस ’70 के दशक तक ही थम जाने वाले नहीं थे। उनकी विद्रोही चेतना उन्हें कृषि प्रधान बिहार के नक्सल आंदोलन की ओर ले गई मास्टर साब और रामेश्वर अहीर जैसे नाम अब इतिहास हो गए हैं।
इस इतिहास को मैं जनवृत्त के साथ खड़ी होकर देखती हूँ ! राजवृत्त के इतिहास के लेखक ऐतिहासिक होते हैं। मैं उन लोगों को ढूँढ़ती रहती हूँ—जिनका कोई नाम नहीं, कोई मुकाम नहीं, जो शोषण के चक्के में पिसते-पिसते एक दिन विद्रोह का शंख फूँक देते हैं। कभी-कभी वे अपनी लड़ाई जीत नहीं पाते और मर भी जाते हैं। उनकी समाधि पर या श्मशान में कोई स्मृति स्तंभ या फलक नहीं लगा होता। लेकिन भारत के इतिहास में मैंने बार-बार होने वाली इस पराजय को कई-कई बार विजय से कहीं अधिक महान पाया है। ग्यारहवीं सदी में बंगाल का कैवर्त-विद्रोह हो या 1857-58 का महाविद्रोह, अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी का संथाल-मुंडा-किसान विद्रोह हो या इस शताब्दी का भारतीय नौ-विद्रोह।
मास्टर साब की कहानी में मैंने उसी लोकवृत्त की भूमिका को लाना चाहा है-जातपाँत का विष और विद्वेष आज भी सक्रिय है और इसीलिए मैंने ऐसी गाथाएँ लिखी हैं।
मैं ऐसे आदमी की कहानी को, अख़्तर-उज़-ज़मान की स्मृति को समर्पित करना चाहती थी। बांग्ला देश में जो महान मुक्ति युद्ध लड़ा गया, उसके पीछे ढाका शहर और सुदूर गाँव के गरीबों ने क्या भूमिका निभाई थी। उसका ही चित्रण उन्होंने अपनी कृति ‘चिलेकोठार सेपाई’ में किया था। इसमें एक नई बांग्ला भाषा थी—शहर और कस्बे की धूल, काँदो-कीचड़-कूड़े और गंदे गटर से लथपथ, तो कहीं धनिक वर्ग की अमानवी असभ्यता से मुखर और झुग्गी-झोंपड़ियों में बंद और कुंद लोगों के एकाएक बारूद बनकर फटने की भाषा। शहर के निचले और पिछड़े तबके के लोगों की बांग्ला भाषा को साहित्य में इतना सम्मान कभी नहीं मिला। जितनी पैनी नजर उतनी ही साफ और सुदृढ़ राजनीतिक आस्था, लोक प्रतिश्रुति से समद्ध तीखा और चुटीला व्यंग्य।
उनके दो उपन्यास हैं—‘चिलेकोठार सेपाई’ और ‘ख्वाबनामा’। कलम ही जिसका हथियार रहा। ये उस योद्धा लेखक की कृतियाँ हैं। मेरी तरह वे भी इस बात से वाकिफ थे कि लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। देश और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लेखक को लड़ना ही पड़ता है। उसे उठ खड़ा होना होता है कट्टरपंथियों के विरुद्ध तथा अपनी अस्मिता और मनीषा को बेच देने के विरुद्ध। लेखकों को वहाँ और अधिक चौकस रहना पड़ता है–जहाँ अँधेरा कुँडली मारे बैठा है। उसे वहाँ प्रकाश फैलाना होता है, अविवेक पर प्रहार और कशाघात करना होता है।
अख़्तर स्वयं एक दुर्दम्य योद्धा थे। 20 जनवरी 1996 को ढाका में मैं उनसे पहली बार मिली थी। कैंसरग्रस्त उनका दाहिना पैर जाँघ से कटा हुआ। मौत सामने खड़ी है और अख़्तर हो...हो हंस रहे हैं। इसके बाद वे भारत के अन्याय भाषाभाषी लेखकों के साथ बड़े आनंद से मिलते रहे, बातें होती रहीं और वे गान सुनते रहे। मैंने वैसा समग्र और जीवंत व्यक्ति नहीं देखा। ऐसा लगता था कि कैंसर रोग भी जैसे उनकी सेवा में खड़ा हो। 4 जनवरी 1997 ने इस युद्धरत सैनिक को हमसे छीन लिया, जिसका हथियार रही उसकी अजेय कलम।
मुझे जो लोग चाहते हैं वे मेरी कृतियों के लिए ही चाहते हैं और उन्हें पता है कि मैं यथासाध्य मनुष्य के लिए ही लड़ाई लड़ रही हूँ। अब आप आवश्य ही समझ जाएँगे कि मैंने यह किताब अख़्तर-उज़-ज़मान इलियास के क्यों समर्पित की है ? आखिर उनके सिवा यह कृति किसी और को कैसे समर्पित की जा सकती थी ? एक योद्धा किसी दूसरे योद्धा के प्रति ही श्रद्धावनत होता है। दूसरे, साहित्य, संस्कृति और ज्ञान के मामले में कहीं कोई सीमारेखा नहीं होती। वे सर्वथा उन्मुक्त क्षेत्र हैं। आकाश का कोई ओर-छोर है ? वह भी तो उन्मुक्त है। अख्तर ने मुझे बाताया कि शोषित लोगों के साथ खड़े होकर उनके लिए काम करते रहना होगा। कलम को विराम देने से काम नहीं चलेगा। मैं इस दायित्व का आजीवन निर्वाह करना चाहती हूँ—अगर जीवन और महाकाल मुझे समय दें।
‘मास्टर साब’, जैसा कि स्पष्ट ही है, एक जीवनीपरक उपन्यास है। मैंने इस से कभी इनकार नहीं किया कि’70 के दशक से जुड़े आंदोलन को मैंने अपना भरपूर समर्थन दिया था। बिहार का आरा जिला वर्ष 1857-58 के दौरान वीर कुअँर सिंह का जिला रहा है। ’70 के दशक में जगदीश मास्टर में धनी जोतदारों द्वारा हरिजन लड़कियों के ऊपर किए जा रहे शोषण और उत्पीड़न के विरुपद्ध अपना प्रतिवाद जताया था। उन्होंने ‘हरिजनिस्तान’ नामक एक गीत-संकलन प्रकाशित किया था और उनके सहोगियों में शहर में एक मशाल जुलूस भी निकाला था। उनका नारा था—‘हरिजनिस्तान लेकर रहेंगे’। यह और कुछ नहीं, रूढ़िवादी अंध-व्यवस्था के विरुद्ध संगठित विद्रोह था और मास्टर साब इस ’70 के दशक तक ही थम जाने वाले नहीं थे। उनकी विद्रोही चेतना उन्हें कृषि प्रधान बिहार के नक्सल आंदोलन की ओर ले गई मास्टर साब और रामेश्वर अहीर जैसे नाम अब इतिहास हो गए हैं।
इस इतिहास को मैं जनवृत्त के साथ खड़ी होकर देखती हूँ ! राजवृत्त के इतिहास के लेखक ऐतिहासिक होते हैं। मैं उन लोगों को ढूँढ़ती रहती हूँ—जिनका कोई नाम नहीं, कोई मुकाम नहीं, जो शोषण के चक्के में पिसते-पिसते एक दिन विद्रोह का शंख फूँक देते हैं। कभी-कभी वे अपनी लड़ाई जीत नहीं पाते और मर भी जाते हैं। उनकी समाधि पर या श्मशान में कोई स्मृति स्तंभ या फलक नहीं लगा होता। लेकिन भारत के इतिहास में मैंने बार-बार होने वाली इस पराजय को कई-कई बार विजय से कहीं अधिक महान पाया है। ग्यारहवीं सदी में बंगाल का कैवर्त-विद्रोह हो या 1857-58 का महाविद्रोह, अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी का संथाल-मुंडा-किसान विद्रोह हो या इस शताब्दी का भारतीय नौ-विद्रोह।
मास्टर साब की कहानी में मैंने उसी लोकवृत्त की भूमिका को लाना चाहा है-जातपाँत का विष और विद्वेष आज भी सक्रिय है और इसीलिए मैंने ऐसी गाथाएँ लिखी हैं।
मैं ऐसे आदमी की कहानी को, अख़्तर-उज़-ज़मान की स्मृति को समर्पित करना चाहती थी। बांग्ला देश में जो महान मुक्ति युद्ध लड़ा गया, उसके पीछे ढाका शहर और सुदूर गाँव के गरीबों ने क्या भूमिका निभाई थी। उसका ही चित्रण उन्होंने अपनी कृति ‘चिलेकोठार सेपाई’ में किया था। इसमें एक नई बांग्ला भाषा थी—शहर और कस्बे की धूल, काँदो-कीचड़-कूड़े और गंदे गटर से लथपथ, तो कहीं धनिक वर्ग की अमानवी असभ्यता से मुखर और झुग्गी-झोंपड़ियों में बंद और कुंद लोगों के एकाएक बारूद बनकर फटने की भाषा। शहर के निचले और पिछड़े तबके के लोगों की बांग्ला भाषा को साहित्य में इतना सम्मान कभी नहीं मिला। जितनी पैनी नजर उतनी ही साफ और सुदृढ़ राजनीतिक आस्था, लोक प्रतिश्रुति से समद्ध तीखा और चुटीला व्यंग्य।
उनके दो उपन्यास हैं—‘चिलेकोठार सेपाई’ और ‘ख्वाबनामा’। कलम ही जिसका हथियार रहा। ये उस योद्धा लेखक की कृतियाँ हैं। मेरी तरह वे भी इस बात से वाकिफ थे कि लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। देश और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लेखक को लड़ना ही पड़ता है। उसे उठ खड़ा होना होता है कट्टरपंथियों के विरुद्ध तथा अपनी अस्मिता और मनीषा को बेच देने के विरुद्ध। लेखकों को वहाँ और अधिक चौकस रहना पड़ता है–जहाँ अँधेरा कुँडली मारे बैठा है। उसे वहाँ प्रकाश फैलाना होता है, अविवेक पर प्रहार और कशाघात करना होता है।
अख़्तर स्वयं एक दुर्दम्य योद्धा थे। 20 जनवरी 1996 को ढाका में मैं उनसे पहली बार मिली थी। कैंसरग्रस्त उनका दाहिना पैर जाँघ से कटा हुआ। मौत सामने खड़ी है और अख़्तर हो...हो हंस रहे हैं। इसके बाद वे भारत के अन्याय भाषाभाषी लेखकों के साथ बड़े आनंद से मिलते रहे, बातें होती रहीं और वे गान सुनते रहे। मैंने वैसा समग्र और जीवंत व्यक्ति नहीं देखा। ऐसा लगता था कि कैंसर रोग भी जैसे उनकी सेवा में खड़ा हो। 4 जनवरी 1997 ने इस युद्धरत सैनिक को हमसे छीन लिया, जिसका हथियार रही उसकी अजेय कलम।
मुझे जो लोग चाहते हैं वे मेरी कृतियों के लिए ही चाहते हैं और उन्हें पता है कि मैं यथासाध्य मनुष्य के लिए ही लड़ाई लड़ रही हूँ। अब आप आवश्य ही समझ जाएँगे कि मैंने यह किताब अख़्तर-उज़-ज़मान इलियास के क्यों समर्पित की है ? आखिर उनके सिवा यह कृति किसी और को कैसे समर्पित की जा सकती थी ? एक योद्धा किसी दूसरे योद्धा के प्रति ही श्रद्धावनत होता है। दूसरे, साहित्य, संस्कृति और ज्ञान के मामले में कहीं कोई सीमारेखा नहीं होती। वे सर्वथा उन्मुक्त क्षेत्र हैं। आकाश का कोई ओर-छोर है ? वह भी तो उन्मुक्त है। अख्तर ने मुझे बाताया कि शोषित लोगों के साथ खड़े होकर उनके लिए काम करते रहना होगा। कलम को विराम देने से काम नहीं चलेगा। मैं इस दायित्व का आजीवन निर्वाह करना चाहती हूँ—अगर जीवन और महाकाल मुझे समय दें।
महाश्वेता देवी
18ए, बालीगंज स्टेशन रोड
कलकत्ता-700019
कलकत्ता-700019
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book